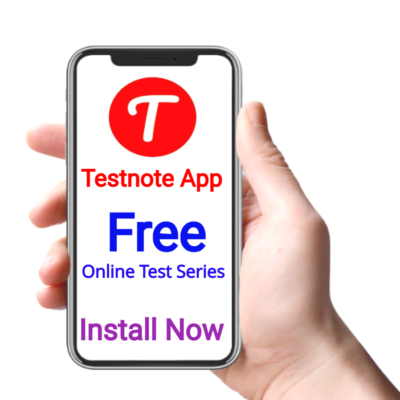संज्ञानात्मक विकास (Cognitive-Development) का सिद्धान्त

- ज्ञानेद्रियाँ विज्ञान के अनुसार 5 होती है आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जो हमें सत्य ज्ञान देती है जिसे संज्ञान कहते है मनोविज्ञान में मन को छठी ज्ञानेन्द्री माना है जिससे प्राप्त ज्ञान असत्य या आभासी हो सकता है |
- जीन पियाजे स्विटजरलैंड के बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने ही बच्चे पर प्रयोग किये | और 1922 से 1932 ई. के बीच जीव विज्ञान के आधार पर बालक के विकास को स्पष्ट किया |
- जीन पियाजे के द्वारा बालक के विकास को जिस तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया उसके अनुसार इन्हें “विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक ” कहते है |
जीन पियाजे का जन्म 1896ई में स्विट्जरलैंड में हुआ। प्याजे ने सर्वप्रथम ‘द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड’ पुस्तक 1923 में लिखी।
पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत-
पियाजे द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है पियाजे ने बताया कि मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास के तीन प्रमुख पक्ष बताए हैं-
- जैविकीय परिपक्वता
- मौलिक पर्यावरण के साथ अनुभव
- सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुभव
- स्कीमा :- यह जीव विज्ञान का शब्द है सरल भाषा में इसका अभिप्राय है क्रिया के समानांतर होने वाली क्रिया जैसे – उद्दीपन – अनुक्रिया | पियाजे के अनुसार संतुलनीकरण ही स्कीमा है। स्कीमा को सही रूप में समझने हेतु इन तीन अवधारणाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है-
- संतुलन / समायोजन / अनुकूलन :- परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या उसके साथ अनुकूलित हो जाना | विकास के लिए संतुलन एक अनिवार्य शर्त है क्योंकि संतुलन ही जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करता है। इसके अभाव में किसी भी प्राणी का विकास संभव नहीं है। पियाजे ने संतुलनीकरण को स्वचालित आरोही प्रक्रिया कहां है जो व्यक्ति के विकास को धीरे-धीरे आगे बढ़ाती रहती है। यह संतुलनीकरण ही पियाजे के अनुसार स्कीमा है। स्कीमा की संरचना की ग्रहिता एक प्रमुख प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में दो तत्व होते हैं-
1. आत्मसातीकरण :- जब एक प्राणी / बालक किसी भी नये विचार या अनुभव को अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ लेता है | या उनके साथ अनुकूलित हो जाता है तो यह आत्मसातीकरण है | आत्मीकरण को किसी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता को कहा जा सकता है जिसके सहयोग से वह नवीन परिस्थिति के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है।
2. समंजन :- समंजन का अर्थ है पूर्व अनुभवों की पृष्ठभूमि में नवीन अनुभवों का आत्मिकरण अर्थात वातावरण से ज्ञान प्राप्त करने में बालक के पूर्व अनुभव भी सहायक होते हैं जो समंजन कहलाते हैं। जब एक व्यक्ति / बालक अपने पुराने अनुभवों का परिमार्जन नये अनुभवों के अनुसार कर लेता है तथा नये विचरों में ढल जाता है |
बालक जैसे-जैसे अपने वातावरण से समंजन और आत्मीकरण करता जाता है उसका संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता जाता है। जीन पियाजे ने स्कीमा के साथ-साथ बालक के बौद्धिक विकास की अवस्थाएं भी बताई है जो कि निम्नलिखित है –
संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ
(1) संवेदी / पेशीय गामक अवस्था या ज्ञानात्मक – क्रियात्मक अवस्था (sensory – motor stage) (जन्म से 2 वर्ष तक) :-
पियाजे के अनुसार यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसे भी पुनः 6 भागों में बांटा गया है।
इस काल को सवेंदी गतिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय में बालक अपने आसपास के पर्यावरण को समझने लगता है।
सारांशतः इस काल में बालक अपना ध्यान किसी चीज पर बहुत ही थोड़े समय के लिए केंद्रित कर सकता है। उसका केवल संवेगात्मक जैसे स्पर्श,स्वाद, गंध, श्रवण, दृश्य आदि का विकास होता है। भाषा के स्थान पर संकेतों का प्रयोग करता है। वह कहने की मुद्रा एवं कहने के ढंग, भावनाओं को समझने लगता है। किस अवस्था के अंत तक अनेक शब्द भी बोल सकता है।
- अनुकरण की अवस्था
- त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ सर्वाधिक सक्रिय
- संवेदनाओं के आधार पर सीखता है |
- इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास हो जाता है | तथा 2 वर्ष का बालक बोलने लगता है |
- वस्तुसमायोजन का ज्ञान तथा अनुक्रिया व परिणाम में सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है |
- वस्तुस्थायित्व :- निश्चित रूप से किसी देखी गई वस्तु या आवाज का स्थायीकरण बालक के मस्तिष्क में होना | यह क्रिया 18 माह के बाद होती है जिसके कारण उसके मस्तिष्क में प्रतिबिम्ब (image) बनने लगते है |
2. प्रतिनिधानात्मक बुद्धि एवं मूर्त संक्रिया काल – यह अवस्था सामान्यत 2 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। पियाजे ने इस अवस्था को पुनः दो भागों में बांटा है-
1. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था / प्राक चलन अवस्था (Pre – Operational stage) (2 से 7 वर्ष तक) :-
यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति रहती है उसका चिंतन साधारण एवं सरल होता है वह भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है।
उदाहरण- एक लंबा तथा दूसरा चौड़ा ग्लास जिसमें बराबर पानी भरा है के बारे में बालक यह तो बता सकता है कि लंबे गिलास में पानी चौड़े गिलास की तुलना में अधिक है परंतु यह नहीं बता सकता है कि दूसरे ग्लास की चौड़ाई अधिक है अतः पानी बराबर है।
- 2 वर्ष की आयु में बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है
- जीववाद / सजीव चिंतन (Animism):- जब एक बालक किसी भी वस्तु को केवल सजीव मानकर व्यवहार करता है |
- आत्मकेन्द्रितता (Egocentrism) :- खुद को राजा समझना |
- स्वनिर्मित भाषा का प्रयोग करना |
- प्रतीकों व प्रतिमाओं के माध्यम से समझना
- खेल व अनुकरण से सीखना
- इस अवस्था में अतार्किक चिन्तन शुरू हो जाता है जो एक विमीय होता है |
जीन पियाजे ने इस अवस्था को दो उपावस्था में बांटा –
(a) पूर्व प्रत्यात्मक काल / पूर्व संकल्पनात्मक काल (2 से 4 वर्ष) :- प्रबल जिज्ञासु काल |
(b) अंत: प्रज्ञ काल / अंत: दर्शी अवस्था ( 4 से 7 वर्ष) :- अनुकरण की अवस्था |
(2) मूर्त संक्रियात्मक अवस्था / ठोस चलन अवस्था / Concrete Stage (7 से 11 वर्ष) :- यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष के मध्य की अवस्था है इस अवस्था में बच्चा अमूर्त एवं तार्किक उदाहरणों को समझने लगता है। बच्चे की आत्म केंद्रित कम होने लगती है एवं पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। इस अवस्था में बालक तथ्यों का सारणीयन वर्गीकरण और अनुरूपीकरण करना प्रारंभ कर देता है।
- पलटावी चिंतन / व्युत्क्रमणशील चिंतन की अवस्था
- गणना से सम्बन्धित प्रारम्भिक अवस्था
- मूर्त वस्तुओं के सन्दर्भ में चिन्तन करना |
- वैचारिक काल अवस्था |
- तार्किक चिंतन का विकास |
- मूर्त अवधारणाओं की पहचान करना, वैचारिक क्रमबद्धता, संधारण / संरक्षण (द्रव्यमान, आयतन,क्षेत्रफल का ज्ञान ), विकेंद्रण (विमाओं का ज्ञान होना) आदि का विकास हो जाता है |
(3) अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था / औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था / Abstract Stage (11 से 16 वर्ष) :- यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की उम्र तक की होती है। इस समय बालक विचार करने की योग्यता चिंतन शक्ति अर्जित कर लेता है। वह अमूर्त संबंधों की विषय में चिंतन कर सकता है एवं समस्या समाधान भी कर सकता है। इस प्रकार यह सउद्देश्य चिंतन की अवस्था है। इस काल में बालक तादात्मीकरण(Identification), निषेधीकरण( Nagation), पारस्परिक संबंधता ( Reciprocalness), तथा सहसंबंध रूपांतरण(Co-relative transformation) ये चार क्रियाऐं करने लगता है जिन्हें पियाजे ने ‘INRC’ के द्वारा अभिव्यक्त किया है।
- पूर्ण परिपक्वता की अवस्था |
- अमूर्त चितन की अवस्था |
- बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास 15 – 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है |
- तार्किकता का उच्चतम स्तर |
पियाजे ने उपरोक्त अवस्थाओं के अतिरिक्त नैतिक और धार्मिक विकास का भी अध्ययन किया तथा पियाजे ने नैतिकता को दो रूप में देखा आश्रित अवस्था एवं स्वायत्त अवस्था तथा आयु वर्गों अनुसार इन्हें पुनः चार अलग-अलग भागों में विभाजित किया है-
नैतिक विकास की अवस्थाएं-
1. आश्रित अवस्था-इस अवस्था में बालक माता-पिता की बातें अनिवार्य रूप से मानते हैं तथा उन सभी बातों या नियमों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इस अवस्था को तीन भागों में बांटा है-
(I) अनौमी-यह अवस्था प्रारंभ से 5 वर्ष तक की अवस्था है इस अवस्था में बालक माता-पिता व समीपजनों के कार्यों की नकल करता है और नैतिक आचरणों में माता-पिता का अनुसरण करता है इसे प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन कहा जाता है वह अपने बड़ों का विरोध नहीं करता तथा उनकी हर बात को स्वीकार करता है।
(II) अधिकारी परायत्ता-5 से 8 वर्ष के मध्य होती है। इसमें बालक समाज द्वारा बताए गए अच्छे नैतिक नियमों को मानने के लिए बाध्य होता है। बालक पुरस्कार एवं दंड द्वारा नियंत्रित होता है। वह अपने सवेंगों पर नियंत्रण रखता है तथा आज्ञाकारी होता है।
(III) परायत्ता– यह अवस्था 9 वर्ष से 13 वर्ष तक की अवस्था होती है इस समय बालक में सहयोग की भावना का विकास होने लगता है उसमें ईमानदारी, न्यायप्रियता, सहयोग और परोपकार जैसी भावनाएं विकसित होने लगती हैं तथा विवेक आ जाता है।
2. स्वायत्ता- यह अवस्था 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था है इस अवस्था में बालक यह समझने लगता है कि नैतिक नियम हमारे व्यवहार के नियामक है यह व्यक्ति के अंतकरण की उपज है अतः बालक अपनी व्यवहारों के प्रति पूर्ण उत्तरदाई होता है। उसका व्यवहार स्वनिर्धारित होता है वह न तो सत्ता द्वारा नहीं समाज द्वारा नियंत्रित होता है बल्कि वह मानवता के आधार पर निर्मित प्रेम सहानुभूति जैसे नैतिक आचरणों के अनुसार चलता है।
General Science
- Sound Question Answers
- ग्रन्थियाँ / Glands Quiz – 05
- ग्रन्थियाँ / Glands Quiz – 04
- ग्रन्थियाँ / Glands Quiz – 03
- ग्रन्थियाँ / Glands Quiz – 02
- ग्रन्थियाँ / Glands
- Nerves System Quiz – 02
- तंत्रिका तंत्र / Nerves System Quiz – 01
- Blood Circulatory System Quiz – 05
- Blood circulatory System Quiz – 02
- रक्त परिसंचरण तंत्र / blood circulatory system – 01
- Respiratory System / श्वसन तंत्र
- Respiratory System / श्वसन तंत्र – 05
- Respiratory System / श्वसन तंत्र – 04
- Respiratory System / श्वसन तंत्र – 03
- Respiratory System / श्वसन तंत्र – 02
- Digestive System Quiz 08
- Digestive System Quiz 07
- Digestive System Quiz 06
- Digestive System Quiz 05
- Digestive System Quiz 04
- Digestive System Quiz 03
- Digestive System Quiz 02
- पोषण एवं पाचन तंत्र Digestive System
- Tissue / उत्तक Quiz – 04
Psychology
- Intelligence Tests
- Other Intelligence theory
- Sampling Theory And Hierarchical Theory
- Multi Factor Theory
- Group Factor Theory
- Spearman’s Two Factor Theory
- Binet’s Uni factor theory
- Intelligence / बुद्धि – 02
- Intelligence / बुद्धि
- Cognitive Development
- Introduction of psychology in Hindi
- child Development
- Educational Psychology : Meaning and Definition / शिक्षा – मनोविज्ञान : अर्थ व परिभाषा
- अधिगम अंतरण के सिद्धांत
- Factors that Affect Learning
- maslow hierarchy of needs theory in Hindi
- Psychology Learning theories
- Psychology Learning Theory (Reinforcement Theory)
- कोहलर का सिद्धांत
- क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत
- शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत
- अधिगम के सिद्धांत
- Learning Part – 01
- Differences Between Growth and Development
- Development in child